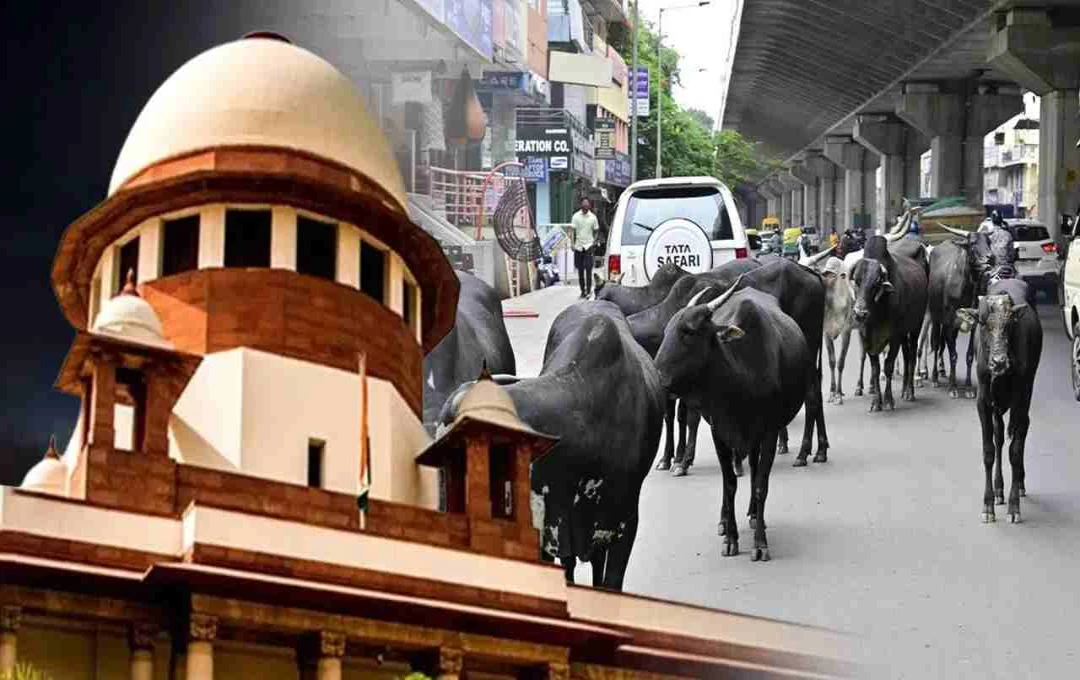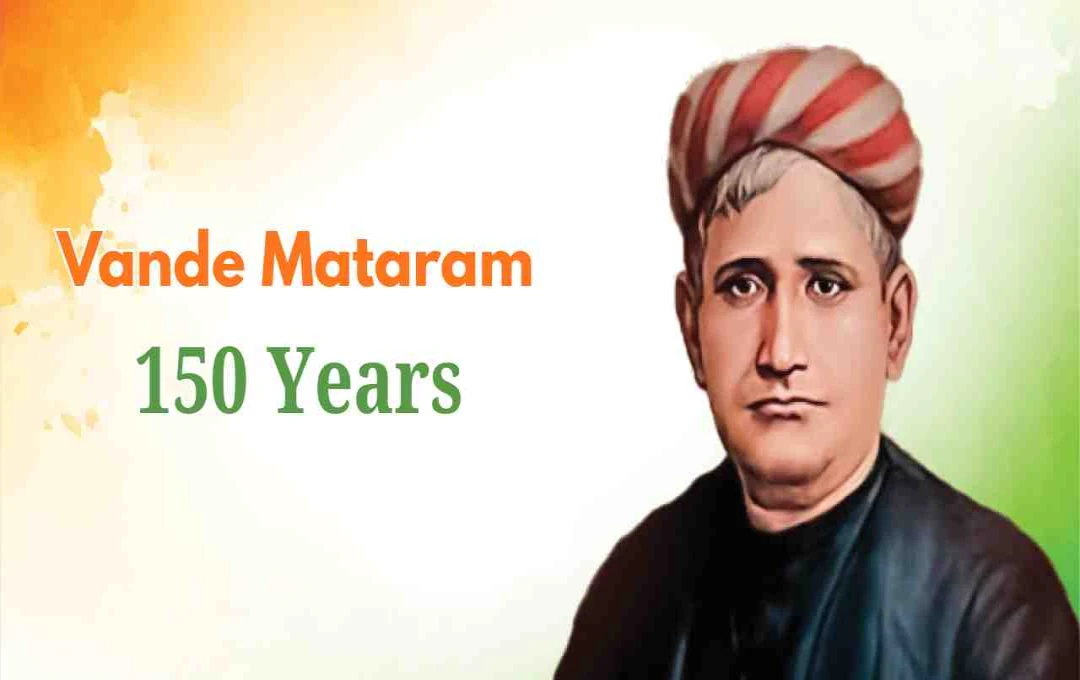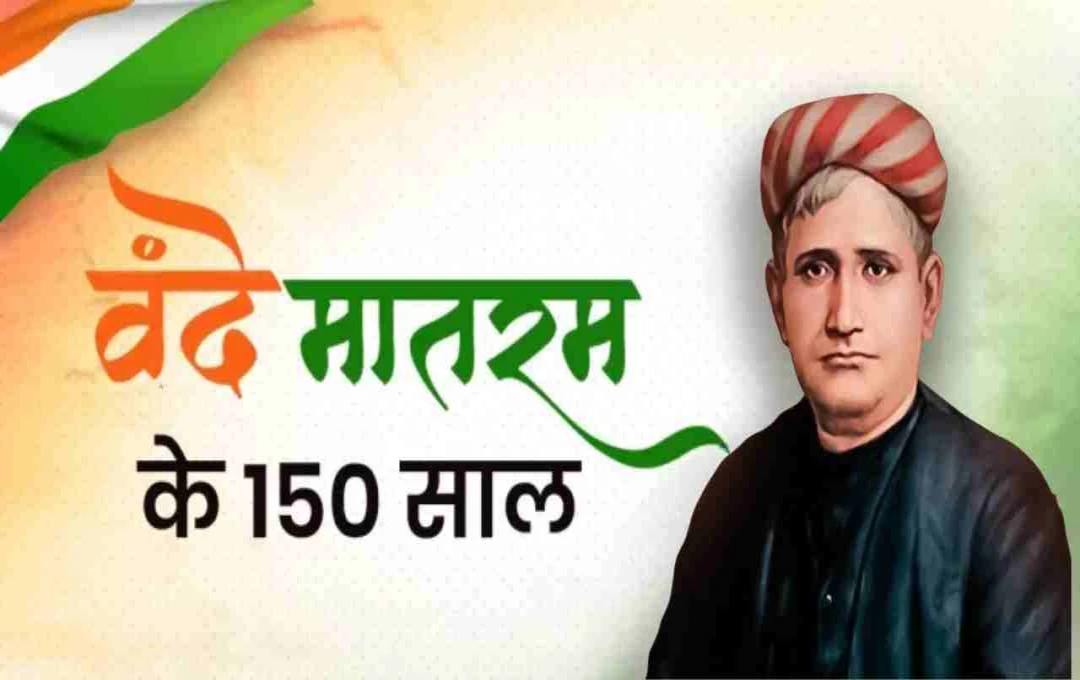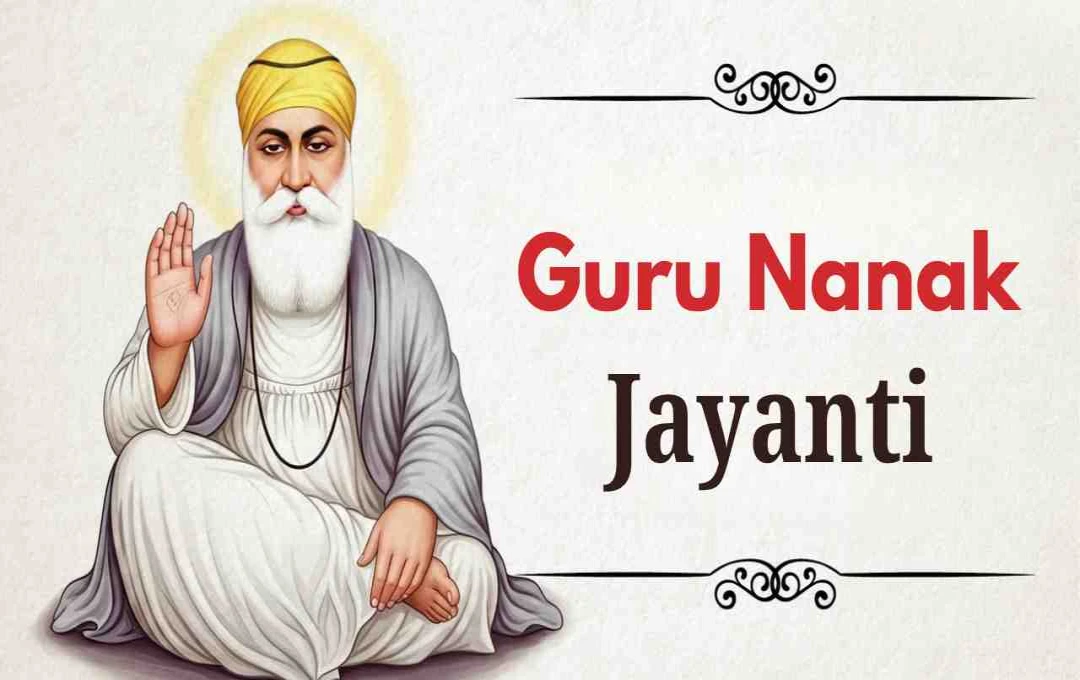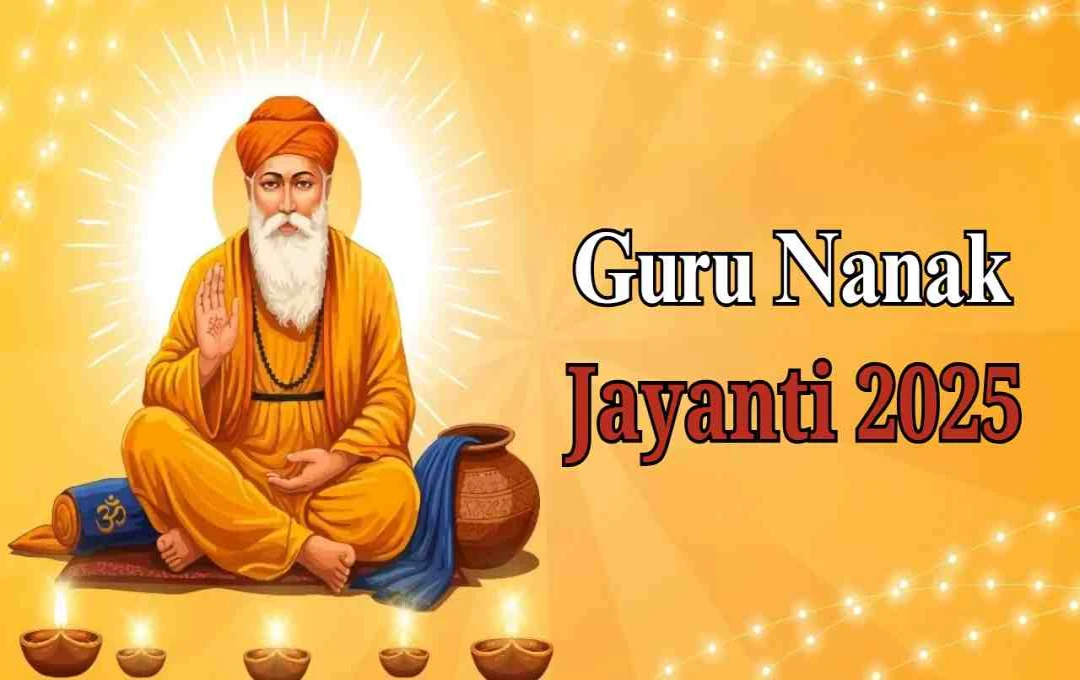भारतीय संसद में 'शून्य काल' यानी Zero Hour एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह वह समय होता है, जब सांसदों को जनहित से जुड़े किसी भी जरूरी और तात्कालिक मुद्दे को बिना पूर्व सूचना के उठाने का अवसर मिलता है।
Zero Hour: भारतीय संसद की कार्यवाही में ‘शून्य काल’ या Zero Hour एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वो समय होता है जब सांसद देश और जनता से जुड़े बेहद जरूरी, संवेदनशील और तत्काल मुद्दों को संसद के पटल पर रखते हैं। हालांकि यह व्यवस्था भारतीय संविधान या संसद के नियम पुस्तिका (Rules of Procedure) में दर्ज नहीं है, लेकिन 1962 से यह परंपरा चली आ रही है।
यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समान रूप से लागू होती है। भारत में संसद का मानसून सत्र हो या शीतकालीन, 'शून्य काल' हमेशा चर्चा का विषय बनता है क्योंकि यहीं से कई बार सरकार को घेरने की शुरुआत होती है।
शून्य काल (Zero Hour) क्यों कहलाता है?
'शून्य काल' का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह प्रश्नकाल (Question Hour) के ठीक बाद और संसद के अन्य आधिकारिक कार्यों से पहले आता है। लोकसभा में यह दोपहर 12 बजे शुरू होता है, इसलिए इसे 'शून्य काल' कहा गया। राज्यसभा में साल 2014 के बाद बदलाव हुआ और अब राज्यसभा में शून्य काल सुबह 11 बजे शुरू होता है।
डिक्शनरी में 'Zero Hour' का अर्थ होता है - ‘निर्णायक समय’ या 'अत्यंत महत्वपूर्ण पल'। संसद में इसका यही महत्व है कि सांसद उस समय सरकार का ध्यान तत्काल मुद्दों पर खींचते हैं।
शून्य काल की शुरुआत कब और कैसे हुई?
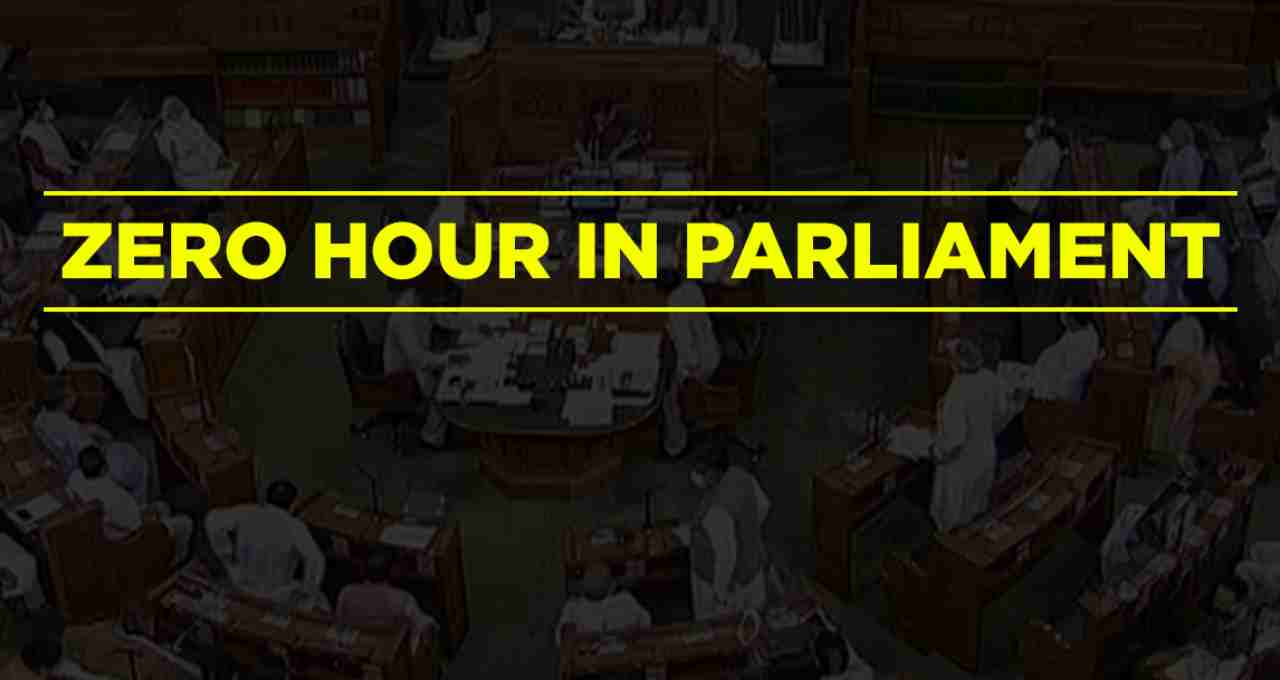
1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान जब संसद का शीतकालीन सत्र जल्दी शुरू हुआ था, तब प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया था। उस समय सांसदों ने तुरंत ध्यान देने योग्य मुद्दों को बिना पूर्व नोटिस के उठाना शुरू किया। तभी से यह परंपरा बनी। नौवीं लोकसभा के स्पीकर रबी रे ने इसे और व्यवस्थित स्वरूप दिया।
उन्होंने यह तय किया कि सांसदों को शून्य काल में मुद्दा उठाने के लिए उसी दिन सुबह 10 बजे तक नोटिस देना होगा और स्पीकर या चेयरमैन तय करेंगे कि कौन से मुद्दे लिए जाएंगे।
शून्य काल कब और कैसे होता है?
लोकसभा में समय
- सुबह 11 बजे से 12 बजे: प्रश्नकाल
- दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे: शून्य काल (Zero Hour)
राज्यसभा में समय (2014 के बाद से)
- सुबह 11 बजे से: शून्य काल
- सुबह 12 बजे से: प्रश्नकाल
शून्य काल की प्रक्रिया (Zero Hour Process)
- नोटिस देना: सांसदों को उसी दिन सुबह 10 बजे तक स्पीकर (लोकसभा) या चेयरमैन (राज्यसभा) के पास लिखित नोटिस देना होता है। इसमें मुद्दा स्पष्ट होना चाहिए।
- मुद्दों का चयन: स्पीकर या चेयरमैन तय करते हैं कि कौन से मुद्दे शून्य काल में उठाए जाएंगे।
- लोकसभा में अधिकतम 20 सांसदों को मौका मिलता है।
- प्राथमिकता जनहित, आपात या संवेदनशील विषयों को दी जाती है।
- समय सीमा: प्रत्येक सांसद को 2-3 मिनट का समय मिलता है। कभी-कभी स्पीकर या चेयरमैन इसे बढ़ा भी सकते हैं।
- सरकारी जवाबदेही: मंत्री चाहें तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन जवाब देना अनिवार्य नहीं होता, जैसा कि प्रश्नकाल में होता है।

शून्य काल का महत्व (Importance of Zero Hour)
- जनता के मुद्दों की तत्काल सुनवाई: सांसद बिना लंबी प्रक्रिया के जनता से जुड़े गंभीर मुद्दे उठा सकते हैं।
- सरकार पर दबाव: चूंकि ये मुद्दे तुरंत उठते हैं, इसलिए सरकार को गंभीरता से सुनना और कभी-कभी फौरन प्रतिक्रिया देना पड़ता है।
- लोकतंत्र को मजबूती: जनता के मुद्दे सीधे संसद में उठाना लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है।
- तुरंत चर्चा का मंच: प्रश्नकाल के बाद शून्य काल ही ऐसा मंच है जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को बिना देरी सामने रखा जा सकता है।
शून्य काल की चुनौतियां (Challenges of Zero Hour)
- अनौपचारिक व्यवस्था: यह संसद के नियमों में शामिल नहीं है, इसलिए कभी-कभी इसका दुरुपयोग भी होता है।
- सीमित समय: सिर्फ 30 मिनट में सभी सांसदों को मौका मिलना कठिन होता है। इससे कई बार असंतोष भी पनपता है।
- संसद में व्यवधान: कभी-कभी भावनात्मक या राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों से संसद का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है और कार्यवाही बाधित होती है।
'शून्य काल' भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सांसदों को जनता की आवाज तुरंत सरकार तक पहुंचाने का मंच देता है। हालांकि यह अनौपचारिक है, फिर भी इसका राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व बहुत अधिक है। इससे सरकार पर जवाबदेही का दबाव बढ़ता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है।