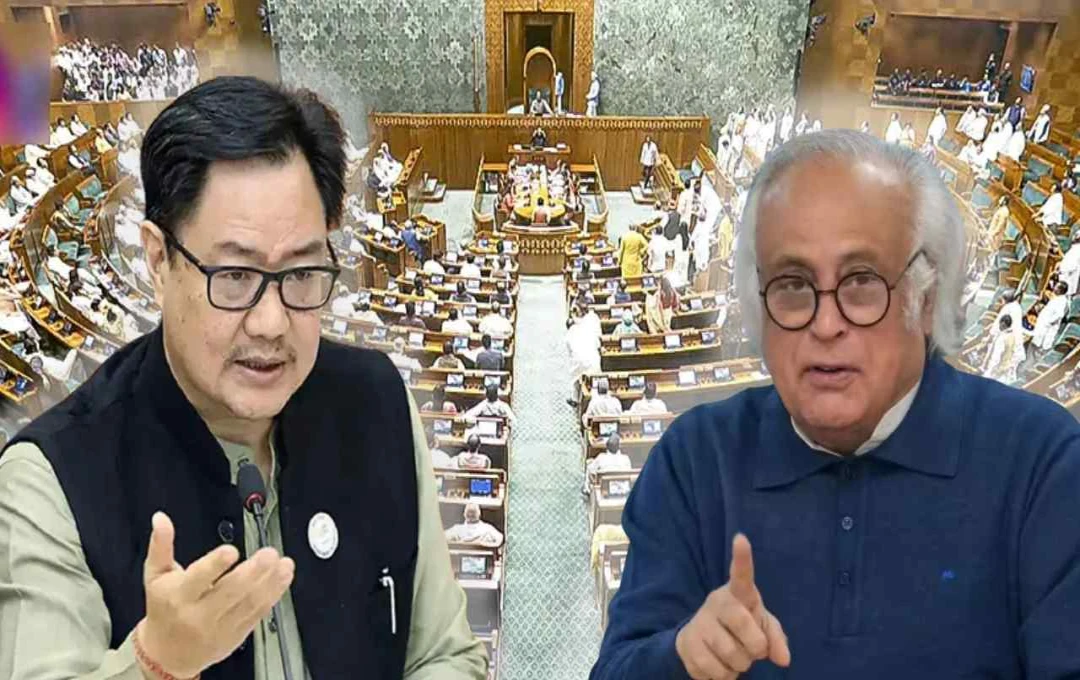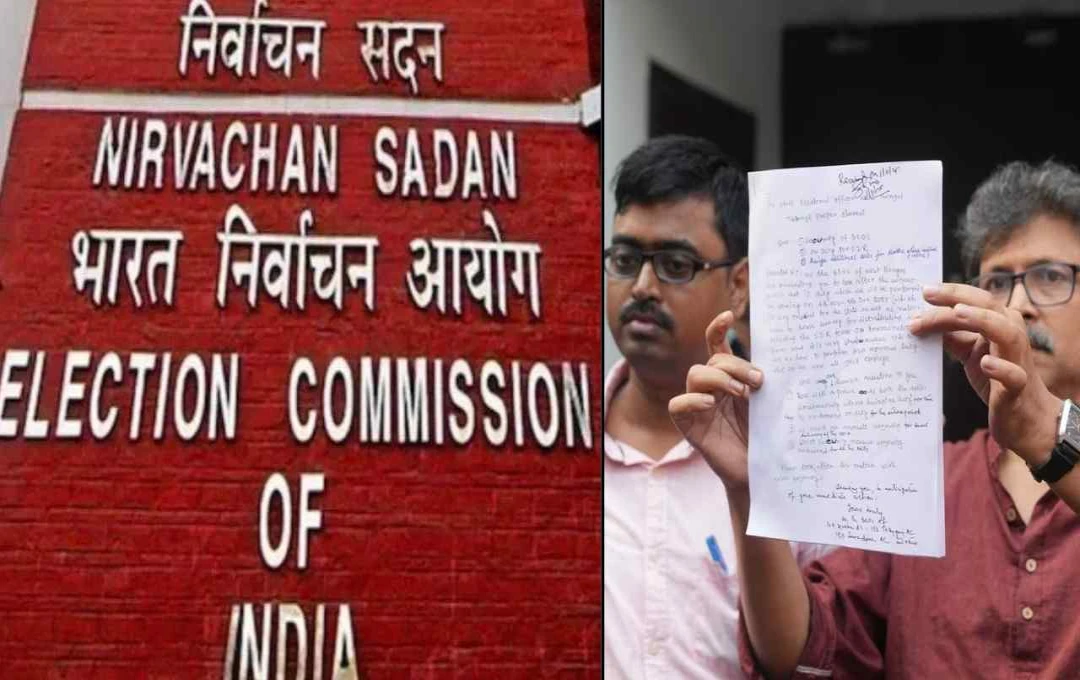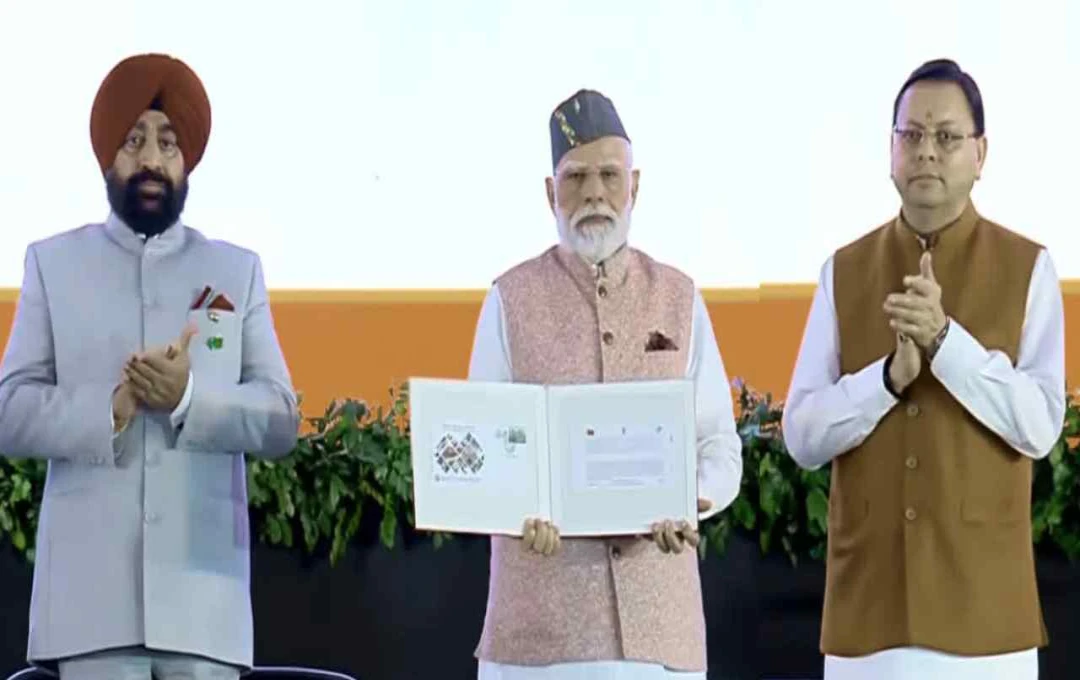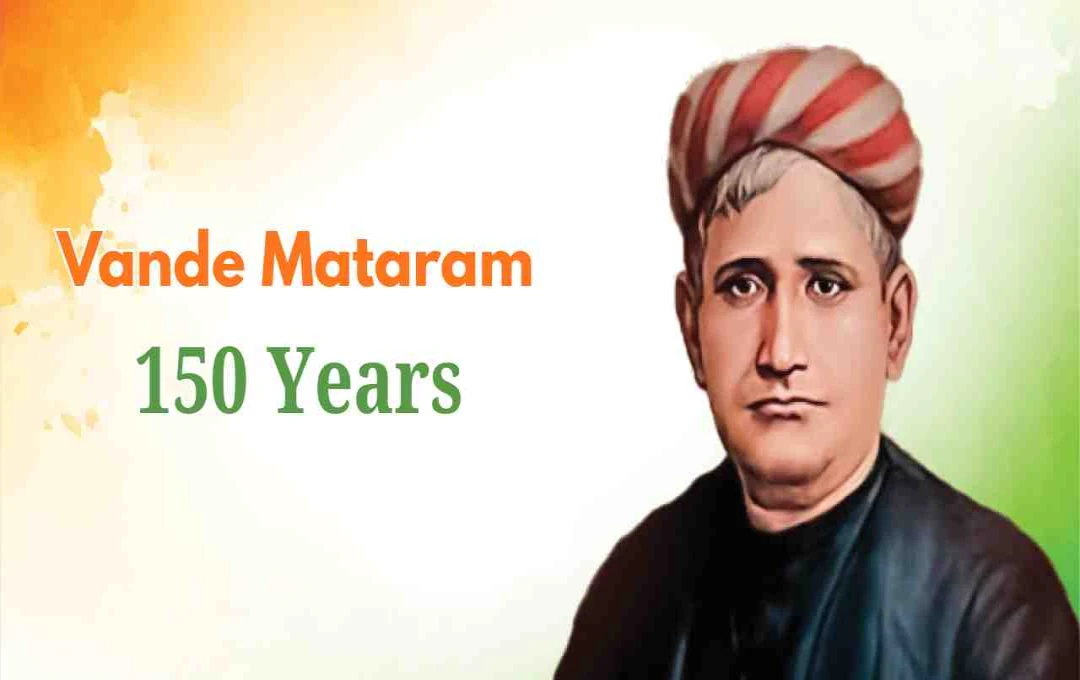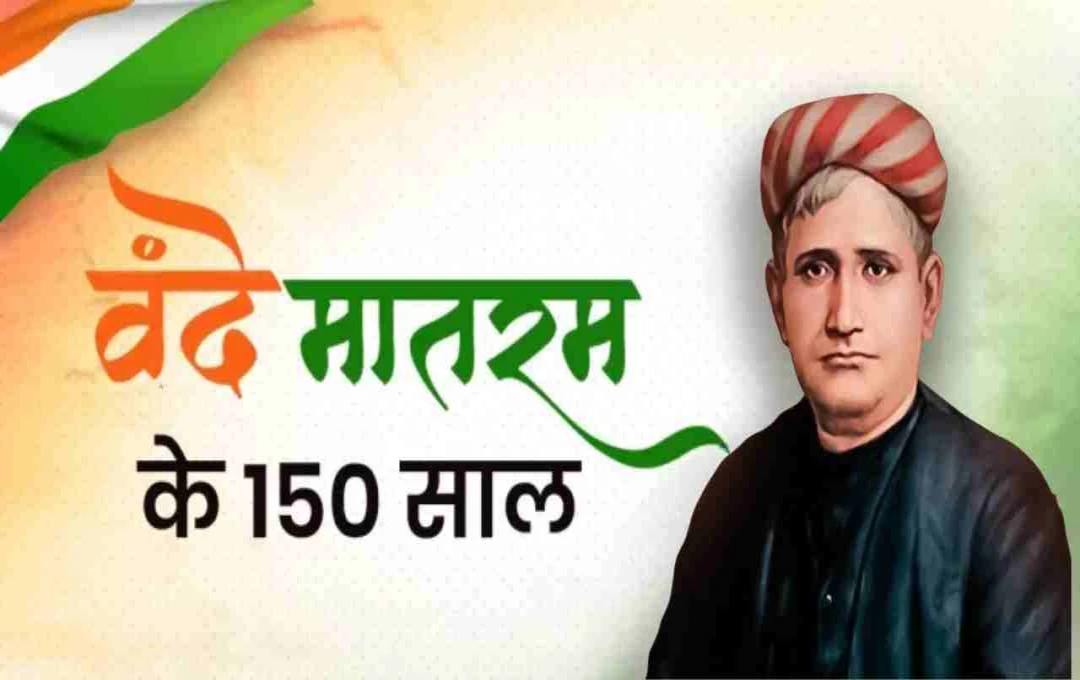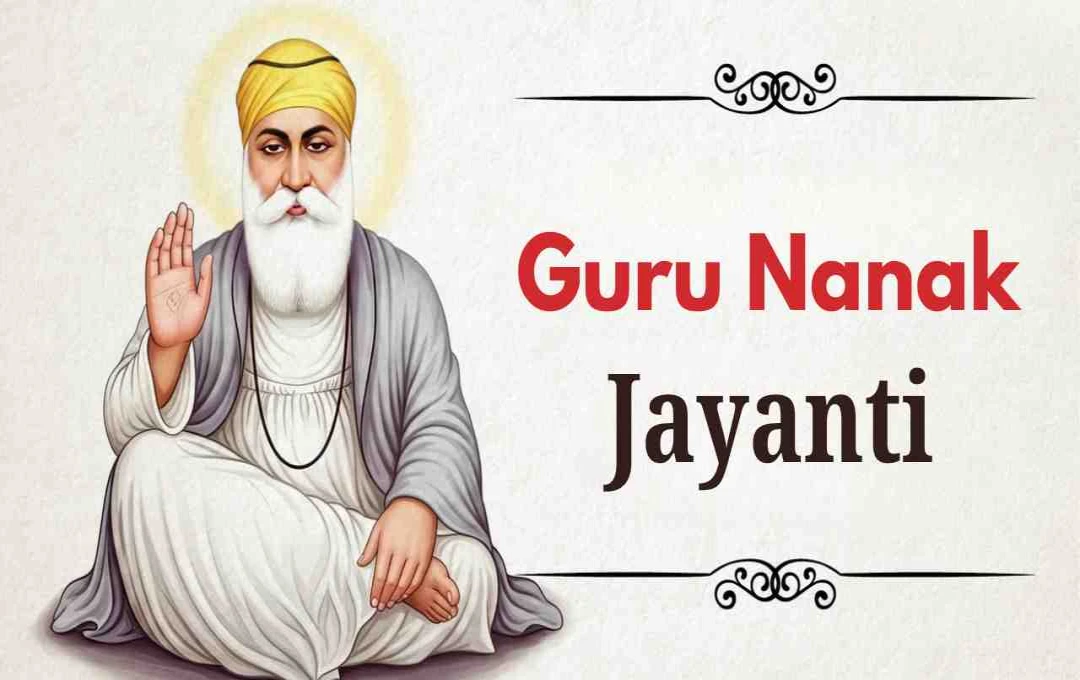भारत की सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राजनीतिक दल यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले POSH एक्ट (Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act, 2013) के दायरे में नहीं आते।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने वाला POSH एक्ट (यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून) राजनीतिक दलों पर लागू नहीं होगा। अदालत ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं को इस कानून के दायरे में लाने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल "कार्यस्थल" की परिभाषा में नहीं आते, और न ही उनके और उनके कार्यकर्ताओं के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध स्थापित होता है। यह फैसला उन महिलाओं के लिए निराशाजनक है जो राजनीति जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें यौन उत्पीड़न से संरक्षण देने वाला कानूनी ढांचा अब उनके लिए उपलब्ध नहीं होगा।
याचिका का उद्देश्य और अदालत का फैसला
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि महिलाओं को हर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए POSH एक्ट का लाभ राजनीतिक दलों और अन्य गैर-पारंपरिक कार्यस्थलों में काम कर रही महिलाओं को भी मिलना चाहिए। याचिका में कहा गया कि कानून की परिभाषा व्यापक रखी गई थी ताकि अधिकतम महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। इसके बावजूद, केरल हाई कोर्ट के मार्च 2022 के फैसले ने कहा था कि राजनीतिक दलों को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं पाया जाता।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों में कार्यरत लोग स्वैच्छिक सदस्य होते हैं और यह संबंध नियोक्ता और कर्मचारी के बीच जैसा नहीं है। इसलिए POSH एक्ट का उद्देश्य वहाँ लागू नहीं होता। अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला नीति-निर्माण से जुड़ा है और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों द्वारा प्रासंगिक दिशा-निर्देश बनाए जा सकते हैं, लेकिन कानून की सीमाएँ स्पष्ट हैं।
POSH एक्ट का उद्देश्य क्या है?
POSH एक्ट की स्थापना 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले के आधार पर की गई थी। इस कानून का मकसद था कि हर कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाव मिले और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए। इसमें नियोक्ता की जिम्मेदारी तय की गई है कि वह एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करे और शिकायतों का समय पर समाधान करे।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कार्यस्थल की परिभाषा में राजनीतिक दल, मीडिया, फिल्म उद्योग जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहें। लेकिन अदालत ने कहा कि कानून की संरचना पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध पर आधारित है, जो राजनीतिक दलों में मौजूद नहीं है।
संविधान और महिला अधिकारों पर असर
याचिका में यह भी कहा गया कि राजनीतिक दलों को POSH एक्ट से बाहर रखना संविधान द्वारा प्रदान समानता (अनुच्छेद 14), भेदभाव निषेध (अनुच्छेद 15), व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(g)) और गरिमा एवं जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि गैर-पारंपरिक कार्यस्थलों में काम कर रही महिलाएं असुरक्षित वातावरण का सामना कर रही हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए।
हालाँकि, अदालत ने यह माना कि नीति निर्माण और सामाजिक जागरूकता के जरिए इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन कानून की परिभाषा में बदलाव करना न्यायिक दायरे से बाहर है। अदालत ने पिछले महीने भी ऐसी ही एक जनहित याचिका खारिज कर दी थी, और याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग से संपर्क करने की सलाह दी थी ताकि राजनीतिक दलों को महिलाओं के लिए शिकायत तंत्र विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सके।